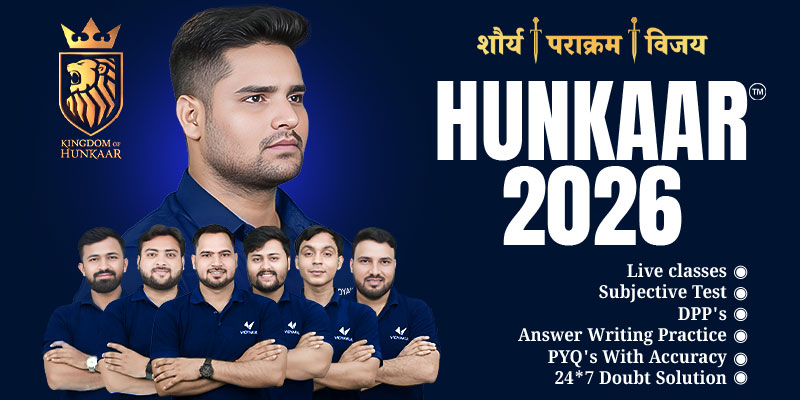बिहार बोर्ड कक्षा 12वी - हिंदी - गद्य खंड अध्याय 9: प्रगीत और समाज के दीर्घ - उत्तरीय प्रश्न
प्रश्न 1: हिंदी की आधुनिक कविता की क्या विशेषताएँ आलोचक ने बताई हैं ?
उत्तर: हिन्दी की आधुनिक कविता में नई प्रगीतात्मकता का उभार देखते है। वे देखते है आज के कवि को न तो अपने अंदर झाँककर देखने में संकोच है न बाहर के यथार्थ का सामना करने में हिचक। अंदर न तो किसी असंदिग्ध विश्वदृष्टि का मजबूत खूटा गाड़ने की जिद है और न बाहर की व्यवस्था को एक विराट पहाड़ के रूप में आँकने की हवस बाहर छोटी-से-छोटी घटना, स्थिति, वस्तु आदि पर नजर है और कोशिश है उसे अर्थ देने की । इसी प्रकार बाहर की प्रतिक्रियास्वरूप अंदर उठनेवाली छोटी-से-छोटी लहर को भी पकड़कर उसे शब्दों में बांध लेने का उत्साह है। एक नए स्तर पर कवि व्यक्तित्व अपने और समाज के बीच के रिश्ते को साधने की कोशिश कर रहा है और इस प्रक्रिया में जो व्यक्तित्व बनता दिखाई दे रहा है वह निश्चय ही नए ढंग की प्रगीतात्मकता के उभार का संकेत है।
प्रश्न 2: आचार्य रामचन्द्र शुक्ल के काव्य-आदर्श क्या थे ? पाठ के आधार , स्पष्ट करें।
उत्तर: आचार्य रामचन्द्र शुक्ल के काव्य आदर्श प्रबंधकाव्य थे क्योंकि प्रबन्धकाव्य में मानव जीवन का एक पर्ण दृश्य होता है। प्रबन्धकाव्य जीवन के सम्पूर्ण पक्ष को प्रकाशित करता है। आचार्य शुक्ल को यह इसलिए परिसीमित लगा क्योंकि वह गीतिकाव्य है। आधनिक का से उन्हें शिकायत भी थी, इसका कारण था-“कला कला” की पुकार, जिसके फलस्वरूप यूरोप में प्रगीत-मुक्तकों (लिरिक्स) का ही चलन अधिक देखकर यह कहा जाने लगा कि अब यहाँ भी उसी का जमाना आ गया है। इस तर्क के पक्ष में यह कहा जाने लगा कि अब ऐसी लंबी कविताएँ पढ़ने की किसी को फुरसत कहाँ है जिनमें कुछ इतिवृत्त भी मिला रहता हो। ऐसी धारणा बन गई कि अब तो विशुद्ध काव्य की सामग्री जुटाकर सामने रख देनी चाहिए जो छोटे-छोटे प्रगीत मुक्तकों में ही संभव है। इस प्रकार काव्य में जीवन को अनेक परिस्थितियों की ओर ले जाने वाले प्रसंगों या आख्यानों की उद्भावना बन्द सी हो गई। यही कारण था कि ज्यों ही प्रसाद की “कामायनी”, “शेरसिंह का शस्त्र समर्पण”, “पंसोला की प्रतिध्वनि”, “प्रलय की छाया” तथा निराला की “राम की शक्तिपूजा” तथा “तुलसीदास’ जैसे आख्यानक काव्य सामने आए तो आचार्य शुक्ल ने संतोष व्यक्त किया।
प्रश्न 3: प्रगीत को आप किस रूप में परिभाषित करेंगे ? इसके बारे में क्या धारणा प्रचलित रही है ?
उत्तर: अपनी वैयक्तिकता और आत्मपरकता के कारण “लिरिक” अथवा “प्रगीत” काव्य की कोटि में आती है। प्रगीतधर्मी कविताएँ न तो सामाजिक यथार्थ की अभिव्यक्ति के लिए पर्याप्त समझी जाती है, न उनसे इसकी अपेक्षा की जाती है। आधुनिक हिन्दी कविता में गीति और मुक्तक के मिश्रण से नूतन भाव भूमि पर जो गीत लिखे जाते हैं उन्हें ही ‘प्रगीत’ की संज्ञा दी जाती है। सामान्य समझ के अनुसार प्रगीतधर्मी कविताएँ नितांत वैयक्तिक और आत्मपरक अनुभूतियों की अभिव्यक्ति मात्र है, यह सामान्य धारणा है। इसके विपरीत अब कुछ लोगों द्वास यह भी कहा जाने लगा है कि अब ऐसी लम्बी कविताएँ जिसमें कुछ इतिवृत्त भी मिला रहता है, इन्हें पढ़ने तथा सुनने की किसी की फुरसत कहाँ है अर्थात् नहीं है।
प्रश्न 4: हिन्दी कविता के इतिहास में प्रगीतों का क्या स्थान है ? सोदाहरण स्पष्ट करें।
उत्तर: हिन्दी कविता का इतिहास मुख्यतः प्रगीत मक्तकों का है। इतना ही नहीं बल्कि गीतों ने ही जनमानस को बदलने में क्रान्तिकारी भूमिका अदा की है। “रामचरितमानस” की महिमा एक निर्विवाद सत्य है, इस सत्य से किसी को इन्कार नहीं, लेकिन ‘विनय-पत्रिका’ के पद एक व्यक्ति का अरण्यरोदन मात्र नहीं है। मानस के मर्मी भी यह मानते हैं कि तुलसी के विनय के पदों में पूरे युग की वेदना व्यक्त हुई है और उनकी चरम वैयक्तिकता ही परम सामाजिकता है। तुलसी के अलावा कबीर, सूर, मीरा, नानक, रैदास आदि अधिकांश संतों ने प्रायः दोहे और गेय पद ही लिखे हैं। यदि विद्यापति को हिन्दी का पहला कवि माना जाय तो हिन्दी कविता का उदय ही गीत से हुआ जिसका विकास आगे चलकर संतों और भक्तों की वाणी में हुआ। गीतों के साथ हिन्दी कविता का उदय कोई सामान्य घटना नहीं, बल्कि एक नई प्रगीतात्मकता (लिरिसिज्म) के विस्फोट का ऐतिहासिक क्षण है जिसके धमाके से मध्ययुगीन भारतीय समाज की रूढ़ि-जर्जर दीवारें हिल उठीं, साथ ही जिसकी माधुरी सामान्य जन के लिए संजीवनी सिद्ध हुई। कहने की आवश्यकता नहीं कि लोकभाषा की परिष्कृत प्रतीकात्मकता का उन्मेष भारतीय साहित्य की अभूतपूर्व घटना है, जिसकी अभिव्यक्ति हिन्दी के साथ ही भारत की सभी आधुनिक भाषाओं में लगभग साथ-साथ हुई।
प्रश्न 5: आधुनिक प्रगीत काव्य किन अर्थों में भक्तिकाव्य से भिन्न एवं गुप्तजी आदि के प्रबन्ध काव्य से विशिष्ट हैं ?
उत्तर: आधुनिक प्रगीत काल का उन्मेष बीसवीं सदी में रोमान्टिक उत्थान के साथ हुआ तथा इसका सम्बन्ध भारत के राष्ट्रीय मुक्ति संघर्ष से है। इसके भक्तिकाव्य से भिन्न इस रोमान्टिक प्रगीतात्मकता के मूल में एक नया व्यक्तिववाद है जहाँ समाज के बहिष्कार के द्वारा ही व्यक्ति अपनी सामाजिकता प्रमाणित करता है। इन रोमान्टिक प्रगीतों में भक्तिकाव्य जैसी तन्मयता नहीं होती किन्तु आत्मीयता और एन्द्रियता उससे कहीं अधिक है। इस दौरान सीधे-सीधे राष्ट्रीयता संबंधी विचारों तथा भावों को काव्यरूप देने वाले मैथिलीशरण गुप्त जैसे राष्ट्रकवि हुए और आधकाशतः उन्होंने प्रबन्धात्मक काव्य ही लिखे जिन्हें उस समय ज्यादा सामाजिक माना गया। रोमांटिक प्रगीत उस युग की चेतना को कहीं अधिक गहराई से वाणी दे रहे थे और उनकी ‘असामाजिकता’ में ही सच्ची सामाजिकता है। इस प्रकार आधुनिक प्रगीतकाव्य भक्तिकाव्य से भिन्न हैं तथा गुप्तजी आदि के प्रबंधकाव्य से विशिष्ट हैं।