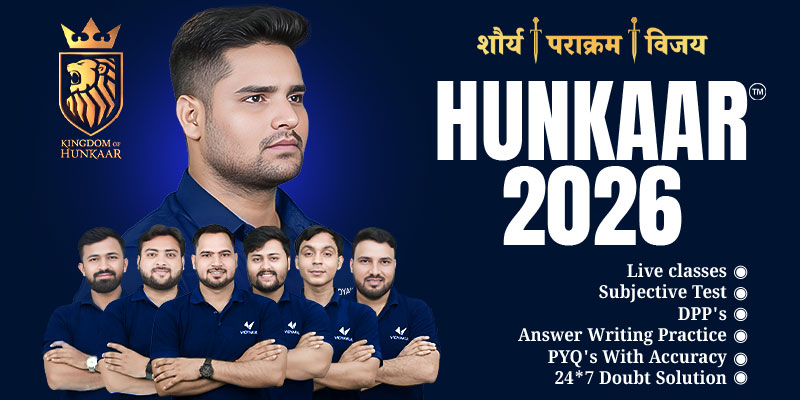बिहार बोर्ड कक्षा 12वी - हिंदी - खंड अध्याय 2: पद - सूरदास के दीर्घ - उत्तरीय प्रश्न
प्रश्न 1: गायें किस ओर दौड़ रही हैं ?
उत्तर: भोर हो गयी है, दुलार भरे कोमल मधुर स्वर में सोए हुए बालक कृष्ण को भोर होने का संकेत देते हुए जगाया जा रहा है। प्रथम पद में भोर होने के संकेत दिए गए हैं. कमल के फूल खिल उठे हैं, पक्षीगण शोर मचा रहे हैं, गायें अपनी गौशालाओं से अपने-अपने बछड़ों की ओर दूध पिलाने हेतु दौड़ पड़ी।
प्रश्न 2: पठित पदों के आधार पर सूर के वात्सल्य वर्णन की विशेषताएँ लिखिए।
उत्तर: सूर के काव्य के तीन प्रधान विषय हैं-विनय भक्ति, वात्सल्य और प्रेम शृंगार। इन्हीं तीन भाब-वृत्तों में उनका काव्य सीमित है। उसमें जीवन का व्यापक और बहुरूपी विस्तार नहीं है, किन्तु भावों की ऐसी गहराई और तल्लीनता है कि व्यापकता और विस्तार पीछे छूट जाते हैं। वात्सल्य के सूर ही विश्व में अद्वितीय कवि हैं। बालक की प्रकृति का इतना स्वाभाविक वर्णन अन्यत्र दुर्लभ है। बाल-स्वभाव के बहुरंगी आयाम का सफल एवं स्वाभाविक चित्रण उनके काव्य की विशेषता है। बालक की बाल सुलभ प्रकृति-उसका रोना, मचलना, रूठना, जिद करना आदि प्रवृत्तियों को उन्होंने अपने काव्य में बड़े मनोवैज्ञानिक ढंग से सजाया है।
पाठ्य-पुस्तक से संकलित पदों में सूरदासजी ने वात्सल्य रस की अनेक विशेषताओं का वर्णन किया है। बालक कृष्ण सोए हुए हैं, भोर हो गई है। उन्हें दुलार से जगाया जा रहा है। जगाने के स्वर भी मधुर हैं। चहचहाते. पक्षियों के, कमल के फूलों के, बोलती और दौड़ती हुई गायों के उदाहरण देकर बालक कृष्ण को जगाने का प्रयास किया जा रहा है।
दूसरे पद में भी वात्सल्य रस की सहज अभिव्यक्ति के क्रम में अनेक विशेषताओं को निरूपित किया गया है। नंद बाबा की गोद में बालक कष्ण भोजन कर रहे हैं। कुछ खा रह हैं, कुछ धरती पर गिरा रहे हैं। बालक कृष्ण को मना-मनाकर खिलाया जा रहा है। विविध प्रकार के व्यंजन दिए जा रहे हैं। यहाँ पर वात्सल्य रस अपने चरम उत्कर्ष पर है। सूरदासजी लिखते है –
“जो रस नंद-जसोदा विलसत, सो नहिं विहँ भवनियाँ।”
प्रश्न 3: सूरदास का कवि परिचय लिखें।
उत्तर: धर्म, साहित्य आर संगीत के संदर्भ में महाकवि सरदास का स्थान न हिन्दी-भाषी क्षेत्र बल्कि सम्पूर्ण भारत में मध्ययुग की महान विभातियों में अग्रगण्य है। यह सूरदास की लोकप्रियता और महत्ता का ही परिणाम है कि ‘सरदास ना किसी भी अच्छी भक्त गाय के लिए रूढ़ सा हो गया है। मध्ययुग में इस नाम के कई भक्त कवि और गायक हो गये है अपने विषय में मध्ययुग के ये भक्त कवि इतने उदासीन थे कि उनका जीवन-वृत्त निश्चित रूप से पुनः निर्मित करना असम्भवप्राय है परन्तु इतना कहा जा सकता है कि सूरसागर के रचयिता सूरदास इस नाम के व्यक्तियों में सर्वाधिक प्रसिद्ध और महान थे और उन्हीं के कारण कदाचित यह नाम उपर्युक्त विशिष्ट अर्थ के द्योतक सामान्य अभिधान के रूप में प्रयुक्त होने लगा। ये सूरदास विट्ठलनाथ द्वारा स्थापित अष्टछाप के अग्रणी भक्त कवि थे और पुष्टिमार्ग में उनकी वाणी का आदर बहुत कुछ सिद्धान्त वाक्य के रूप में होता है।
सूरदास का जन्म संभवतया 1492 ई. में दिल्ली के निकट ‘सीही’ नामक ग्रामक में हुआ था। सूरदास विषय में जो भी ज्ञात है, उसका आधार मुख्यतया ‘चौरासी वैष्णवन की वार्ता’ है। ‘चौरासी वैष्णवन की वार्ता’ में सूर का जीवनवृत गऊ घाट पर हुई बल्लभाचार्य से उनकी भेंट के साथ प्रारम्भ होता है। गऊ घाट पर भी उनके अनेक सेवक उनके साथ रहते थे तथा ‘स्वामी’ के रूप में उनकी ख्याति दूर-दूर तक फैल गयी थी। कदाचित इसी कारण एक बार अरैल से जाते समय बल्लभाचार्य ने उनसे भेंट की और उन्हें पुष्टिमार्ग में दीक्षित किया। बल्लभाचार्य ने उन्हें श्रीमद्भागवत पुराण की कथा सुनाई और विनय के पद रचने के लिए कहा। सूर ने भागवत के द्वादश स्कन्ध के पदों पर पद-रचना की। उन्होंने जो सहस्त्रावधि पद रचे जो ‘सागर’ कहलाये। सूरदास की पद-रचना और गान-विधा की ख्याति सुनकर अकबर ने उनसे मिलने की इच्छा व्यक्त की। तानसेन की मदद से मिले भी सूर बड़े विनम्र स्वभाववाले मृदुभाषी व्यक्ति थे। सूरदास की सर्वसम्मत प्रामाणिक रचना ‘सूरसागर’ है। सूरसागर के अलावा साहित्य लहरी और ‘सूरसागर सारावली’ है।
सूरदास के काव्य से उनके बहुश्रुत अनुभव सम्पन्न विवेकशील और चिन्तनशील व्यक्तित्व का परिचय मिलता है। उनका हृदय गोप बालकों की भाँति सरल और निष्पाप ब्रज गोपियों की भाँति सहज संवेदनशील प्रेम-प्रवण और माधुर्यपूर्ण तथा नन्द और यशोदा की भाँति सरल विश्वासी, स्नेह-कातर और आत्मबलिदान की भावना से अनुप्राणित था। साथ ही उनमें कृष्ण जैसी गम्भीरता और विदग्धाता तथा राधा जैसी वचन चातुरी और आत्मोत्सर्गपूर्ण प्रेम विवशता थी। काव्य में प्रयुक्त पात्रों के विविध भावों से पूर्ण चरित्रों का निर्माण करते हुए वस्तुतः उन्होंने अपने महान व्यक्तित्व की ही अभिव्यक्ति की है। उनकी प्रेम-भक्ति के सख्य वात्सल्य और माधुर्य भावों का चित्रण जिन असंख्य संचारी भावों अनगिनत घटना-प्रसंगों बाह्य जगत प्राकृतिक और सामाजिक के अन्त सौन्दर्य चित्रों के आश्रय से हुआ है। उनके अन्तराल में उनकी गम्भीर वैराग्य-वृति तथा अत्यन्त दीनतापूर्ण आत्म निवेदात्मक भक्ति-भावना की अन्तर्धाय सतत प्रवहमान रही है परन्तु उनकी स्वाभाविक विनोदवृति तथा हास्य प्रियता के कारण उनका वैराग्य और दैन्य उनके चित को अधिक ग्लानियुक्त और मलिन नहीं बना सका। आत्महीनता की चरम अनुभूति के बीच भी उल्लास व्यक्त कर सकें। उनकी गोपियों विरह की हृदय विदारक वेदना को भी हास-परिहास के नीचे दबा सकीं। करुण और हास का जैसा एकरस रूप सूर के काव्य में मिलता है अन्यत्र दर्लभ है। सूर ने मानवीय मनोभावों और चितवृतियों को लगता है नि:शेष कर दिया है। सूरदास प्रमुख रूप से वात्सल्य रस के अप्रतिम कवि हैं। प्रस्तुत पद में भी इसकी झाँकी मिलती है।
प्रश्न 4: सूरदास रचित पद शीर्षक कविता का सारांश लिखें।
उत्तर: इस पद में दुलार भरे कोमल मधुर स्वर में सोए हुए बालक कृष्ण को भोर होने की सूचना देते हुए यह कहा जा रहा है कि हे ! ब्रजराज नंद के पुत्र ! जागिए ! कमल के फूल खिल उठे, कुमुदिनियों का समूह संकुचित हो गया, भ्रमर लताओं को भूल गए। मुर्गे तथा अन्य पक्षियों के कोलाहल को सुनो जो पेड़ों पर बोल रहे हैं। गायें बाड़ों में रँभाने लगी है और बछड़ों के लिए दौड़ रही है। चन्द्रमा फीका पड़ गया, सूर्य का प्रकाश फैल गया। स्त्री-पुरुष गा रहे हैं। कमल सदृश हाथों वाले श्याम उठो, अब प्रात:काल हो गया।
श्याम नंद की गोद में बैठे भोजन कर रहे हैं। वे कुछ खाते हैं, कुछ भूमि पर गिराते हैं। इस छवि को नंदरानी देख रही है। बड़ी, बड़ा बेसन के बहुत से प्रकार तथा विविध प्रकार के अनगिनत व्यंजन हैं। वे अपने हाथों से लेकर डालते हुए खा रहे हैं। दही के दोनों की ओर उनकी विशेष रुचि है। मिश्री, दही और मक्खन को मिलाकर छवि के घानी कृष्ण मुख में डालते हैं। वे आप भी खाते हैं और नंद के मुख में भी डालते हैं। इस छवि का वर्णन करते नहीं बनता। इस प्रकार जो आनन्द नंद और यशोदा पा रहे हैं वह तीनों लोकों में नहीं है। कृष्ण भोजन करके जब आचमन (कुल्ला ) किया तो सूरदास जूठन माँग रहे हैं।”
प्रश्न 5: सूरदास की भक्ति भावना पर प्रकाश डालिए।
उत्तर: सगुण भक्ति धारा की कृष्णाश्रयी शाखा के अग्रगण्य कवि सूरदास की भक्ति-भावना में बल्लभाचार्य का चिंतन और पुष्टि-मार्गी भावना की झलक मिलती है। शंकराचार्य के निर्गुणवादी चिन्तन का विरोध स्वभावतः हो जाता है क्योंकि सूरदास शंकराचार्य के विरोधी बल्लभाचार्य के शिष्य हैं। बल्लभाचार्य ने सगुण को ही असली पारमार्थिक रूप बतलाया और निर्गुण को उसका अंशतः तिरोहित रूप कहा। सूरदास ने अपने विनय के पदों में जिस भक्ति-भावना की व्यंजना की है उसमें बल्लभ की उपर्युक्त बातें स्पष्ट हैं। उन्होंने जीव अर्थात् भक्त की दयनीयता
और ईश्वर की सर्वशक्तिमता को व्यजित किया है। उन्होंने यह भी बतलाया कि निर्गुण का कोई रूप-गुण और आकार नहीं होती है। इसलिए उसके प्रति हमारी आस्था स्थापित होना सम्भव नहीं है। आखिर मनुष्य अपनी विपदाओं की बात किसे कहे ? निर्गुण तो अगोचर है। उसे जो जानता है वही समझ सकता है। वह अनुभवगम्य है, उसे परखना सबसे सम्भव नहीं । इसलिए तो उन्होंने कहा –
रूप-रेख-गुन-जाति-जुगुति-बिनु निरालम्ब मन चक्रित धावै । सब विधि अगम अगोचर विचारहिं तातें सूर सगुन लीला पद गावै ॥
सूरदास की भक्ति में एकनिष्ठ समर्पण और आत्म-निवेदन का भाव है। सूर को कृष्ण की लीला का ज्ञान है, उनकी महिमा का ज्ञान है और है अपनी भक्ति पर अभिमान। उन्होंने कृष्णभक्ति के प्रति अपनी एकनिष्ठता दिखाते हुए कहा है कि ‘मेरो मन अनंत कहा सुख पावै।’ कहने का तात्पर्य यह है कि सगुण के अलावे अन्य मतों पर उनका कतई विश्वास नहीं है। वे तो केवल सगुण रूप श्रीकृष्ण के उपासक हैं। मन-पंछी के लिए सगुण रूप कृष्ण उस जहाज की तरह हैं जो विशाल सागर के बीच उतर चला है। इतना ही नहीं, सगुण अगर गंगा है तो निर्गुण कूप, सगुण अगर कमल और कामधेनु है तो निर्गुण करील और बकरी के समान है। इतजनी असमानता होने पर कोई मूढमति क्यों निर्गुण की बात करेगा?
कमल नैन को छाड़ि महातप और देव को ध्यावै।
परमगंग को छाड़ि पियासो दुरमति कूप खनावै॥
जिहिं मधुकर अम्बुज-रस चाख्यौ, क्यो करील फल भावै।
सूरदास प्रभु कामधेनु तजि छेरी कौन दुहावै॥
सूरदास की भक्ति-भावना में सांसारिकता अर्थात् काम-क्रोध, मद-मोह आदि भावनाओं का निराकरण आवश्यक है। इन दुर्गुणों से पोषित मानव-मन हमेशा दुखी रहता है। जब तक सांसारिक वृत्तियों में आदमी बँधा हुआ है तब तक उसके भीतर विपदाओं की पीडा रहेगी। लेकिन इस अविद्या का नाश तभी हो सकता है जब भगवान की कृपा हो जाय
“अब मैं नाच्यौ बहुत गोपाल।काम-क्रोध को पहिरि चोलना, कंठ विषय की माल ॥
महामोह के नूपुर बाजत, निन्दा शब्द रसाल ।
भ्रम-भर्यो मन भयौ पखावज, चलत असंगत चाल ॥
कोटि कला काछि दिखराई, जल-थल सुधि नहीं काल ।
सूरदास की सबै अविद्या दूरि करौ नन्दलाल ।”
सूरदास की भक्ति-भावना में ईश्वर सभी कर्मों का कर्ता माना गया है। संसार की सारी क्रियाओं का वही नियंता है। जीव तो निमित्त मात्र है। अपने पुरुषार्थ पर. अहंकार करने वाला जीव सचमुच मूढ़मति है। ईश्वर ने जो कुछ लिखा है वही होगा –
“करी गोपाल की सब होई।जो आपन पुरुषारथ मानत, अति झूठौ है सोई॥
साधन, मंत्र, जंत्र, उद्यम, बल ये सब डारौ दोई।
जो कुछ लिखि राखि नन्दनन्दन, मेटि सकै नहिं कोई॥”
सूरदास ने यह स्वीकार किया है कि सम्पूर्ण सृष्टि ब्रह्म की लीला के लिए आत्मकृति है। वह अपने को असंख्य जीवों में बिखेर कर लीला करता है। भक्ति की साधना के लिए बल्लभ ने जिस प्रेम-लक्षणा भक्ति की बात कही, सूरदास ने उसे अपने साहित्य में स्थापित किया। इसका प्रमाण हमें उनके “भ्रमरगीत” में मिल जाता है।
संक्षेप में कहा जा सकता है कि सूरदास की भक्ति-भावना में पुष्टिमार्गीय भक्ति है जिसमें बल्लभाचार्य का चिंतन दिखायी पड़ता है। उनकी भक्ति में प्रेम-लक्षणा भक्ति की झलक मिलती है। इनके ‘विनय’ में इनकी विनयशीलता सचमुच हृदय को छू जाती है। इसके साथ-साथ सूरदास ने अपनी भक्ति में सांख्य भाव को स्थापित किया है, जिसके लिए वे प्रसिद्ध माने जाते हैं।
हिंदी के सभी अध्याय के महत्वपूर्ण प्रशन उत्तर के लिए अभी Download करें Vidyakul App - Free Download Click Here