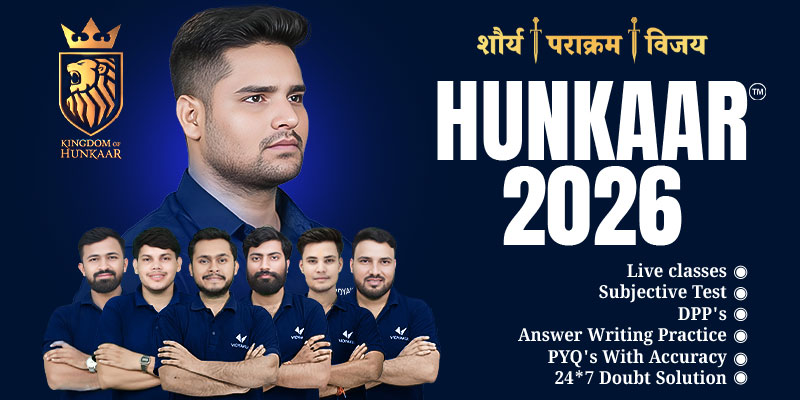बिहार बोर्ड कक्षा 12 जीव विज्ञान अध्याय 16 पर्यावरण के मुद्दे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न
दीर्घ उत्तरीय प्रश्न
प्रश्न 1. वातावरण को ताप तथा वायुमण्डलीय गैस किस प्रकार प्रभावित करते हैं?
उत्तर-- वातावरण एक सन्तुलित व्यवस्था है जिसमें इसे बनाने वाले सभी भौतिक तथा जैविक कारक अपना एक सन्तुलन बनाये हुए हैं। इस वातावरण में उपस्थित विभिन्न जैव समुदाय जिसमें मनुष्य भी सम्मिलित है, पर इसे बनाने वाले भौतिक कारको में किसी प्रकार का परिवर्तन उसके जैविक घटकों को प्रभावित करता है। कुछ उदाहरण निम्नलिखित है-
1. ताप : ताप भी पृथ्वी पर सामान्यतः सूर्य के प्रकाश से ही प्राप्त होता है, किन्तु इसके अतिरिक्त भी ताप के अन्य स्रोत माने गये हैं; जैसे— पृथ्वी स्वयं ही ताप का स्रोत है। सूक्ष्म जीवों आदि के द्वारा उत्पन्न ताप भी इसमें वृद्धि करता है। यद्यपि ये सब भी किसी न किसी रूप में सूर्य से ही इस ताप को प्राप्त करते हैं। सामान्यतः पौधे 0°C से ऊपर तथा 50°C से नीचे जीवित रहते हैं, फिर भी इससे नीचे या ऊपर सुषुप्त हो सकते हैं। बीजों, बीजाणुओं आदि के अंकुरण से लेकर वृद्धि तथा परिवर्द्धन की लगभग सभी क्रियाओं पर ताप का निश्चित प्रभाव पड़ता है, यद्यपि अंकुर पर यह प्रभाव अधिक स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर होता है अर्थात् जीवों को सभी जैव क्रियाओं पर पड़ता है। प्रौढ़ होने पर धीरे-धीरे यह प्रभाव कम होता जाता है। इस दृढीकरण कहते हैं। कुछ पौधों के बीजों तथा कलियों को खिलने से पूर्व कुछ समय तक अधिक या कम ताप की एक दशा में रखना आवश्यक होता है। गेहूं के सम्बन्ध में इस प्रकार के प्रयोगों से महत्वपूर्ण परिणाम प्राप्त हुए है बसन्तीकरण इसी प्रकार की क्रिया है। पौधों के भौगोलिक वितरण पर भी तापमान का प्रभाव पड़ता है। भूमध्य रेखा से धुवों की और समुद्रतल से पहाड़ों की ऊँचाई की ओर वनस्पति के प्रकार का क्रम क्रमशः ताप की कमी के कारण एक होता है।
2. वायु तथा इसकी गैसें- वायु में उपस्थित गैसे पौधे के उपयोग में आने के अतिरिक्त अनेक प्रकार से भू-जैव-रासायनिक चक्रों को बनाती है, जिससे विशेषकर पौधों व अन्य को अनेक प्रकार की सुविधायें प्राप्त होती हैं। प्रकाश संश्लेषण, श्वसन, नाइट्रोजन स्थिरीकरण आदि क्रियायें से चलते रहने के लिए इन गैसों का सन्तुलित अवस्था में रहना आवश्यक है। कुछ गैसों की अवचित मात्रा अतिरिक्त व अवांछित गैसों से वायु का प्रदूषण होने पर जीवों को जीवन-यापन में कठिनाई हो सकती है उनमें विशेष प्रभाव उत्पन्न हो सकते है।
प्रश्न 2. प्राकृतिक सन्तुलन में वृक्षों का योगदानबताए,
उत्तर: पर्यावरण को सन्तुलित रखने में वृक्षों का अत्यधिक योगदान है। वृक्ष अनेक प्रकार के प्राकृतिक चक्रों को चलते रहने में सहायता करते हैं; जैसे—कार्बन चक्र, ऑक्सीजन चक्र, जल चक्र, अनेक खनिज पदार्थों आदि ये खाद्य श्रृंखलाओं के लिए उत्पादक है और इनका अन्य कोई विकल्प नहीं है। (वनस्पति) सभी जीवों द्वारा श्वसन में उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करके प्रकाश संश्लेषण द्वारा इसे खा पदार्थों में बदलते है। इस प्रकार ये पर्यावरण से कार्बन डाइऑक्साइड को हटाते हैं और बदले में जीवों को स्वपन की क्रिया को चलाये रखने के लिए प्राणदायक ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं। इस प्रकार जीवन की दो प्रमुख आवश्यकताओं भोजन तथा शुद्ध वायु के लिए वृक्षों (वनस्पति) का होना अनिवार्य है।
उपर्युक्त के अतिरिक्त वृक्षों के होने से मृदा ढकी रहती है, अत: उसका जल तथा वायु द्वारा अपरदन नहीं हो पाता है। यदि वृक्ष न हो तो बाद आने का खतरा होता है। वनों की कमी से वर्षा कम होती है। वायु को तेज गति को रोकने में वृक्ष बहुत सहयोग करते हैं।
स्पष्ट है, वृक्ष जलवायु सम्बन्धी अनेक कारकों, मृदीय कारकों तथा जैवीय कारकों को भिन्न-भिन्न प्रकार से प्रभावित करके सन्तुलित करते हैं तथा पर्यावरण को सन्तुलित रखते हैं।
प्रश्न 3. औद्योगीकरण से मानव जीवन पर क्या प्रभाव होता है?
उत्तर- औद्योगीकरण से मानव जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। औद्योगिक संस्था से अनेक प्रकार के प्रदूषक जैसे-जैसे ठोस कण तथा अन्य विषैले पदार्थ वायु जल में मिलते रहते हैं। इनसे भिन्न प्रकार के भयानक रोग उत्पन्न हो सकते है अथवा ये रोग की प्रतिरोधक शक्ति को कम कर देते हैं जिससे अनेक रोगों के रोगाणु शरीर पर आक्रमण कर रोग उत्पन्न कर सकते हैं। प्रदूषक पदार्थों में जिसमें का नाइट्रोजन के विभिन्न ऑक्साइड्स जैसे सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक कार्बन के कण, सीसा, आर्सेनिक आदि हो सकते हैं। यह आसाद या फेफड़ों के अनेक रोग, आँखा के साधारण और असाधारण रोग उत्पन्न करते हैं। इनसे पाचन तथा उत्सर्जन अनेक रोग हो सकते हैं। प्रदूषक कैंसर जैसे रोग के लिए अनुकूल परिस्थितियां बनाते है। कावट, मानसिक तनाव हड्डी और दाँत के रोग, रक्त चाप आदि इनके प्रभाव से हो सकते है। प्रतिरोधक शक्ति के कम होने से अनेक रोगों के रोगाणु शरीर पर आक्रमण करके शीघ्र ही रोगी बनाते हैं।
प्रश्न 4. ओजोन परत पर टिप्पणी लिखे।
उत्तर: ओजोन परत या ओजोन मण्डल:
हमारे पृथ्वीं रूपी पिण्ड के चारों और उपस्थित विभिन्न गैसों आदि का आवरण अर्थात् वायुमण्डल लगभग 14-16 हजार किमी ऊँचाई तक है। इसका धरातल से केवल 800 किमी ऊँचाई तक का भाग जीवों के लिए अत्यधिक महत्त्वपूर्ण है। तापमान तथा वायुदाब के आधार पर वायुमण्डल को क्षोभमण्डल जिसमें हम रहते हैं, समताप मण्डल जिसमें ओजोन मण्डल है, आदि भागों में बांटते हैं। ओजोन परत जिसे ओजोन मण्डल कहते हैं, समतापमण्डल के निचले तथा क्षोभमण्डल के ऊपरी (बाहरी) भाग में स्थित है। इस भाग में 15 से 30 किमी ओजोन गैस (O)) की एक मोटी परत होती है। यह गैस ऑक्सीजन के तीन परमाणुओं से बनी हुई तथा इससे ही मिलती-जुलती होती है। इसमें एक विशेष प्रकार की तीखी गंध होती है तथा इसका रंग नीला होता है। ओजोन सूर्य से आने वाली हानिकारक किरणों प्रमुखतः पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी रूपी मुख्य पिण्ड पर आने से रोककर पृथ्वी और उसके जीवधारियों के सुरक्षा कवच के रूप में कार्य करती है।
ओजोन गैस के क्षरण से यह परत पतली हो जाती है तथा इस पतले (thin) परत वाले स्थान को ओजोन छिद्र कहते हैं। अनेक सर्वेक्षणों के अनुसार ओजोन परत लगातार पतली हो रही है। तथा उसमें छिद्र बन रहे हैं यही नहीं बने हुये छिद्रों का विस्तार हो रहा है। ब्रिटेन के अण्टार्कटिका सर्वेक्षण दल (1985) ने अपने अनुभवों और शोध के आधार पर अण्टाकाटिका में हेली खाड़ी के ऊपर ओजोन गैस की अधिक कमी बतायी है। इस रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि 1977 से 1984 के मध्य इस क्षेत्र में ओजोन में लगभग 40% की कमी आयी है। जापान के वैज्ञानिकों के आधार पर 1981 की अपेक्षा 1991 में ओजोन छिद्र हही तेरह गुना अधिक विस्तृत हो गया है। 1992 की एक रिपोर्ट के अनुसार उत्तरी गोलार्द्ध के घनी आबादी वाले क्षेत्रों में ओजोन परत अनुमान के विपरीत दोगुनी गति से पतली होती जा रही है। दूसरा ओजोन छिद्र, आर्कटिक महासागर के ऊपर बताया गया है जो आबादी रहित क्षेत्र में होने के कारण अभी अधिक समस्या दायक नहीं है।
प्रश्न 5. भूमंडलीय उषमयन के कारण बताए।
उत्तर: ऊष्मारोधी ग्रीन हाउस गैसो की वायुमण्डल में अधिक बढ़ोत्तरी निम्नांकित कारणों से हुई है- 1. औद्योगीकरण – औद्योगीकरण तथा घरों में जीवाश्म ईंधनों, जैसे- कोयला, पेट्रोलियम आदि पदार्थों के उपयोग में वृद्धि के कारण वायुमण्डल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस में अत्यधिक वृद्धि हुई है। लगभग 18000 वर्ष पूर्व हिमनद काल से अन्तर्हिमनद युग तक CO2 गैस में 40% की वृद्धि हुई है। औद्योगिक क्रान्ति से पूर्व वायुमण्डल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 280 ppm थी जो 1991 में बढ़कर 353 ppm हो गई; ग्रीन हाउस प्रभाव में इस गैस का योगदान 60% से अधिक है। अतः इन तथ्यों से प्रकट होता है कि. औद्योगीकरण ग्रीन हाउस प्रभाव में एक महत्त्वपूर्ण कारण रहा है।
2. वनों का विनाश या वनोन्मूलन — जनसंख्या वृद्धि आदि कारणों से विश्व में प्रतिवर्ष लगभग 7 करोड़ हैक्टेयर भूमि से वनों को हटाया जा रहा है। यदि वन विनाश की यही दर रही तो इस शताब्दी के अन्त तक विश्व के 5% भूभाग पर ही बन रहना सम्भव हो सकेगा। वनों के विनाश से अनेक प्रकार की हानियाँ होती है, जिनमें पर्यावरण में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कमी आती है, परिणामस्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर सन्तुलित नहीं रहता है। वर्तमान दर से वनोन्मूलन द्वारा वृक्षों के विनाश से प्रतिवर्ष दो अरब टन अतिरिक्त कार्बन डाइऑक्साइड वायुमण्डल में आती है। वृक्ष कार्बन डाइऑक्साइड को कम करने में सहायक होते हैं जिन्हें हम विनष्ट करते जा रहे हैं। स्पष्टतः ग्रीन हाउस प्रभाव में वृद्धि अवश्यम्भावी है।
3. क्लोरोफ्लोरो कार्बन का उपयोग- हम जनते है कि क्लोरोफ्लोरो कार्बन एवं मेथेन गैसों का ग्रीन हाउस प्रभाव की वृद्धि में 90% तक योगदान सम्भव है। इसका प्रमुख कारण है कि ये गैसें समतापमण्डल में उपस्थित ओजोन पर्त को नष्ट करती हैं। ओजोन पर्व ही पृथ्वी पर पराबैंगनी किरणों को आने से रोक पाने में समर्थ है अन्यथा इसमें उपस्थित घातक विकिरण पृथ्वी पर अनेकानेक हानिकारक प्रभाव उत्पन्न कर देगा। आजकल इन गैसों का प्रयोग अनेक प्रकार के वातानुकूलन उपकरण, रेफ्रिजरेटरों, गद्देदार सीटों आदि में काम आने वाली फोम, इंजिन्स, सुगन्धित कॉस्मेटिक ऐरोसॉल स्प्रे आदि के निर्माण में किया जाता है। इन गैसों का प्रयोग छोटे-छोटे इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों आदि की सफाई में भी किया जाता है।
प्रश्न 6. चिपको आंदोलन को संक्षेप मे बताए।
उत्तर: चिपको आन्दोलन:
सन् 1730 ई० के सितम्बर माह में राजस्थान के जोधपुर जिले के जोधपुर से 21 किमी दक्षिण-पूर्व में ि खेजड़ली ग्राम के वृक्षों को ईंधन के लिये काटने के आदेश वहाँ के महाराजा अभयसिंह द्वारा दिये गये। ग्राम को महिलाओं ने पेड़ों को काटने वाले व्यक्तियों से पेट्रों को न काटने का काफी अनुरोध किया इसका आरम्भ श्रीमती अमृता देवी विश्नोई व उसकी तीन पुत्रियों ने किया। कारिन्दों द्वारा उनकी बात न मानने पर विरोध में वृक्षों में चिपक कर 363 स्त्री-पुरुषों ने अपने प्राणों की आहुति दे दी। राजा को इसका ज्ञान हुआ तो उन्होंने वृक्षों को काटने के आदेश वापस ले लिये। इस ग्राम में इन शहीदों की स्मृति में प्रतिवर्ष एक मेले का आयोजन किया जाता है।
स्वतन्त्रता प्राप्ति से पूर्व उत्तरकाशी (अब उत्तराखण्ड में है) केतिलाड़ी ग्राम में भी इसी प्रकार जन आन्दोलन | पर्यावरणीय सचेतना के साथ इसी प्रकार का जन आन्दोलन गढ़वाल के सुदूर ग्रामीण क्षेत्र के रेणनी नामक 1 से 1972 में प्रारम्भ हुआ। इसे चिपको आन्दोलन की संज्ञा दी गई। इसका नेतृत्व एवं प्रसार श्री सुन्दर लाल हुआ। स्थान ब्रहुगुणा एवं श्री चण्डी प्रसाद भट्ट द्वारा किया गया। इस आन्दोलन के अन्तर्गत क्षेत्रीय ग्रामीण महिलाओं ने पेड़ों को बचाने के लिये ठेकेदारों व पुलिस से संघर्ष किया। 'चिपको' शब्द महिलाओं की भावनात्मक पुकार थी जो वृक्षों के बचाव हेतु संघर्ष करते-करते मुँह से निकली इस आन्दोलन के अन्तर्गत महिलायें पेड़ों से चिपक कर मजदूरों को कुल्हाड़ी से पेड़ों को बचातीं। धीरे-धीरे यह वृक्ष बचाओ अभियान एक आन्दोलन के रूप में सम्पूर्ण उत्तराखण्ड में फैल गया।
स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद उत्तराखण्ड हिमालय के वन संसाधनों का विनाश बड़ी तीव्रता से हुआ जिससे भागीरथी नदी घाटी व अलकनंदा नदी घाटी में बाढ़, भूस्खलन तथा सूखे की घटनायें बढ़ने लगीं। अनेक ग्राम वासियों द्वारा वन विनाश का निरन्तर विरोध किया गया। इसी सन्दर्भ में 1970 में उत्तरकाशी में "गंगोत्री ग्राम स्वराज्य संघ" तथा गोपेश्वर (चमोली) गढ़वाल में 'देशोली ग्राम स्वराज्य संघ' की स्थापना करके सरकार को वन नीतियों का विरोध किया गया। ऊपरी अलकनंदा घाटी में 12000 वर्ग किलोमीटर को पारिस्थितिकीय दृष्टि से नाजुक क्षेत्र घोषित किया गया। रेणनी ग्राम इसी क्षेत्र में है।
चिपको आन्दोलन के उद्देश्य- इस आन्दोलन के दो प्रमुख उद्देश्य रहे हैं-
1. आर्थिक स्वावलम्बन के लिये वनों का व्यापारिक दोहन बन्द किया जाये।
2. प्राकृतिक सन्तुलन स्थापित करने हेतु वृक्षारोपण के कार्यों को गति दी जाये ।।
प्रश्न 7. ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन में ध्यान रखने योग्य बातें कौन कौन सी है?
उत्तर: ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन में निम्नांकित बातों का ध्यान रखना आवश्यक है:
1. ठोस अपशिष्टों को नियमित रूप से एकत्रित करना प्रथम चरण है। इसके लिए प्रत्येक नगर की प्रत्ये गली- कालोनी में निश्चित स्थान पर कूड़ादान रखा जाए तथा वहाँ एकत्र कचरे को नियमित रूप से उठाया जाए।
2. विघटनीय एवं अविघटनीय कचरे का संग्रहण पृथक-पृथक किया जाए, ताकि उनका निपटान एवं चक्रण में सुविधा रहे। सड़ा-गला भोजन, फल, सब्जियाँ आदि विघटनीय पदार्थ की श्रेणी में आते हैं।
3. किसी प्रकार के अपशिष्ट का खुले में सन्निक्षेपण न किया जाये।
4. एकत्रित समस्त कूड़े-करकट को प्रतिदिन सन्निक्षेपण स्थल तक पहुंचाने के समुचित उपाय नगर निका द्वारा किए जाए।
5. नगरों के व्यस्त क्षेत्रों (बाजार, सार्वजनिक स्थल आदि) में कचरे का संग्रहण प्रतिदिन एक से अधिक बार किया जाए।
6. अपशिष्ट पदार्थों को एकत्रित करने के बाद उनका समुचित निस्तारण या निपटान महत्त्वपूर्ण कार्य है। एकत्रित कचरे की छँटाई करके तथा उन्हें विभिन्न श्रेणियों में वर्गीकृत करके विघटनीय पदार्थों को गड्ढों में एकत्र कर खाद बनायी जा सकती है। ज्वलनशील पदार्थों एवं अज्वलनशील अपशिष्टों को आबादी वाले क्षेत्रों या जल क्षेत्रों में दूर बनाये गए सन्निक्षेपण स्थलों पर ही डालना उचित है।
7. ज्वलनशील अपशिष्टों के निपटान हेतु नगर निकायों द्वारा भस्मकों की स्थापना करना उचित प्रक्रिया है।
8. ठोस अपशिष्टों का समुचित निस्तारण न करने वाली संस्थाओं एवं व्यक्तियों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही की जानी चाहिए तथा नगर में रहने वाले नागरिकों को भी कम मात्रा में ठोस अपशिष्ट पपदार्थों के उत्सर्जन की सलाह एवं प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए।
9. भारत कृषि प्रधान देश है अतः कृषि अपशिष्टों की मात्रा यहाँ अधिक होती है। यद्यपि कृषि अपशिष्ट अधिक हानिकारक नहीं होते किन्तु अधिक मात्रा में इनका एकत्रित होना कठिनाई का सबब हो सकता है। विशेषकर पशुओं द्वारा उत्सर्जित अपशिष्टों तथा कृषि कार्य में प्रयुक्त रासायनिक पदार्थों के अवशेष एवं उनके पैकिंग मैटीरियल)।
10. कृषि अपशिष्ट अनेक प्रकार से आर्थिक रूप में लाभदायक सिद्ध होते हैं; जैसे—इनसे बायोगैस या अन्य गैसें बनाकर ऊर्जा की समस्या को काफी हद तक हल किया जा सकता है। इसी प्रकार कृषि अपशिष्टों का प्रबन्ध उन्हें पुनः चक्रित करके किया जा सकता है इससे अत्यधिक आर्थिक लाभ भी होता है।
11. नगरीय अपष्टि से कागज, काँच, धातुयें, प्लास्टिक, कार्बनिक पदार्थ आदि की छंटाई, संग्रहण आदि करके विभिन्न संसाधना को पुनः प्राप्ति करके पुनः चक्रित किया जा सकता है।
12. प्लास्टिक विशेषकर PVC तथा पॉलीथीन का प्रयोग तथा उससे उत्पन्न अपशिष्ट अत्यन्त दुविधाजनक है। इनका पुन:चक्रण भी अनेक प्रकार से मनुष्य तथा जन्तुओं के स्वास्थ्य को हानि पहुँचाने वाला होता है।
प्रश्न 8. जल प्रदूषण के स्त्रोत व दुसप्रभाव बताए।
उत्तर: जल प्रदूषण के स्त्रोत:
1. कृषि इत्यादि में प्रयोग किये गये कीटाणुनाशक एवं कीटनाशक; जैसे—डी०डी०टी० व पी०सी०बी० आदि।
2. सीसा (Pb) व पारा (Hg) के कार्बनिक व अकार्बनिक यौगिक जो औद्योगिक संस्थानों से निकलते हैं।
3.मनुष्यों द्वारा वाहित मल जिसमें अनेक रोगकारक होते हैं।
4.भूमि पर गिरने वाला या तेल वाहकों द्वारा ले जाने वाले तैलीय पदार्थ तथा अनेक प्रकार के वाष्पीकृत होने वाले पदार्थ; जैसे—पेट्रोल, एथीलीन, | ट्रेटाक्लोर, तेल आदि जो वायुमण्डल से द्रवित होकर जल में आ जाते हैं।
5.रेडियोधर्मी पदार्थ; जैसे - कार्बन - 14, स्ट्रॉन्शियम - 90, सीजियम-137, आयोडीन - 131 आदि जो परमाणु विस्फोटों आदि से उत्पन्न होते हैं। और जल प्रवाह में पहुँचते हैं।
दुसप्रभाव:
1. जलीय प्राणियों; जैसे-मछलियों आदि पर विषैला - प्रभाव तथा इन्हें खाने पर मनुष्य के मस्तिष्क पर विषैला प्रभाव और यकृत के कैन्सर की सम्भावना में वृद्धि।
2. जलीय पौधों एवं प्राणियों पर विषैला प्रभाव तथा | मछलियों आदि की मृत्यु व मानव तन्त्रिका तन्त्र पर विषैला प्रभाव।
3.. मनुष्यों में विभिन्न रोग; जैसे—टाइफॉयड, हैजा, पेचिश, पीलिया आदि ।
4. जलीय वनस्पति का विनाश, बड़ी संख्या में | मछलियों की मृत्यु से आर्थिक क्षति। इस प्रकार के जलीय प्राणियों को खाने से अनेक रोगों की सम्भावना। जल में ऑक्सीजन की कमी, हाइड्रोकार्बन्स से विभिन्न रोग।
5. रेडियोधर्मी जल अथवा जलीय प्राणियों के सेवन से मनुष्यों में ल्यूकीमिया व कैन्सर जैसे घातक रोगों की सम्भावना।
प्रश्न 9. जेव आवर्धन पर संक्षेप मे टिप्पणी दे।
उत्तर: जैव आवर्धन— जैव आवर्धन या जैव विस्तार वह प्रक्रिया है जिसमें विषैले पदार्थ, जिनका विनष्टीकरण नहीं होता उच्च पोषी स्तरों में क्रमश: सान्द्रित होते रहते हैं जिससे उच्चतम मांसाहारी में इन पदार्थों की अत्यधिक सान्द्रता बन जाती है।
जैव आवर्धन का सर्वोत्तम उदाहरण डी०डी०टी० (DDT) जैसे पदार्थों का प्रयोग है। ये पदार्थ जैव शरीर में उपापचित नहीं होते। ऐसे पदार्थ जल में प्रायः अघुलनशील होते हैं तथा वसाओं में विलेय। इनका इस कारण से मूत्र के साथ भी उत्सर्जन नहीं होता है। इस प्रकार शाकाहारी द्वारा खाया गया ऐसा पदार्थ (जैसे DDT) इसके शरीर के अन्दर मांस में एकत्र होता रहता है और जब उच्च पोषी स्तर वाले मांसाहारी द्वारा उसका भक्षण किया जाता है तो वह इस मांसाहारी के शरीर में पहुँच जाता है। इस प्रकार यह एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में पहुँचता रहता है। इस प्रकार क्रमिक पोषी स्तरों पर DDT की सान्द्रता बढ़ जाती है। जैसे यदि जल में इसकी सान्द्रता यदि 0.001 पी०पी०बी० (ppb parts per billion) से प्रारम्भ होती है तो अन्त में जैव आवर्धन के द्वारा मत्स्यभक्षी पक्षियों में बढ़कर 25 ppm हो जाती है।पक्षियों में DDT की उच्च सान्द्रता कैल्सियम उपापचय को हानि पहुंचाती है जिससे अण्ड कवच पतला हो जाता है; फलस्वरूप अण्डा समय से पहले ही फट जाता है। स्पष्ट है इसके फलस्वरूप पक्षी- समष्ट घटती जायेगी। उदाहरण- ब्राउन पेलिकॉन पक्षी इसी कारण संकटग्रस्त हो गया है।
प्रश 10. प्रकाश रासायनिक ध्रूम क्या है? व किस प्रकार से जन जीवन को प्रभावित करता है?
उत्तर: प्रकाश रासायनिक- ऑक्सीकारक प्रकाश रासायनिक धूप-कोहरा :
वायु की जल वाष्प, कोहरा आदि धुर्वे के साथ मिलकर धूम्र कोहरा बनाती है। इसमें 80 ऑक्सीजन से क्रिया करके SO, बनाती है तथा जल वाष्प के साथ यह अम्ल में बदल जाता है। इसी प्रकार कुछ पदार्थ वातावरण में आने पर अन्य पदार्थों से क्रिया करके अन्य प्रकार के विषैले पदार्थ, द्वितीयक प्रदूषक बना लेते हैं जो स्वास्थ्य पर हानिकारक प्रभाव डालते हैं। उदाहरण के लिए वाहनों से निकलने वाले अदग्ध हाइड्रोकार्बन तथा नाइट्रोजन ऑक्साइड सूर्य के प्रकाश में प्रतिक्रिया कर लेते हैं तथा प्रकाश-रासायनिक स्मॉग का निर्माण करते हैं। इस परॉक्सी एसीटिल नाइट्रेट तथा ओजोन होते हैं। इस प्रकार बनने वाले पदार्थ विषैले होते हैं। मनुष्य पर PAN का प्रभाव विशेषकर आँखों तथा श्वसन पथ पर होता है। खाँसी, सिर दर्द, अधिक थकान, रक्त स्राव, गले का शुष्क होना आदि तथा साँस लेने में कठिनाई हो जाती है। पौधों के लिए भी ये हानिकारक होते हैं, PAN के प्रभाव से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया अवरुद्ध हो जाती है। ओजोन पत्तियों में श्वसन तेज कर देती है। यह पत्तियों में कांस्यन तथा क्लोरोसिस पैदा करती है। पत्तियों का असमय गिरना, जड़ तथा तनों की वृद्धि में कमी, पौधों की समय पूर्ण जीर्णता तथा बीजों के उत्पादन में कमी आदि लक्षण ओजोन से पैदा हो सकते है। पौधे भोजन की कमी से नष्ट हो जाते हैं। अब, यह भी ज्ञात हुआ है कि ओजोन के प्रभाव से मीसोफिल कोशिकाओं का जीवद्रव्य तथा केन्द्रक सिकुड़ जाते हैं, अन्तरकोशिकीय स्थान बढ़ जाता है तथा कई पौधों में विभिन्न रोगों के लिए यह उत्तरदायी है; जैसे—पत्तियों के शीर्ष जलना, प्याज की अग्रिम कोशिकाओं का जलना, सेम का कांस्यन, आलू की पत्तियों पर धब्बे, अंगूर की पत्तियों का भूरा होना।
हिंदी के सभी अध्याय के महत्वपूर्ण प्रशन उत्तर के लिए अभी Download करें Vidyakul App - Free Download Click Here