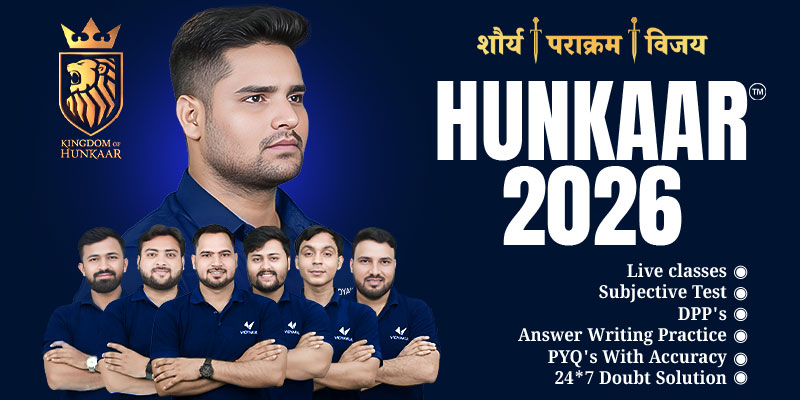बिहार बोर्ड कक्षा 12 जीव विज्ञान अध्याय 8 मानव स्वास्थ्य ऍवम रोग लघु उत्तरीय प्रश्न
लघु उत्तरीय प्रश्न
प्रश्न 1. ऐण्टीजेन्स तथा एण्टीबॉडीज में अन्तर स्पष्ट कीजिए।
उत्तर- ऐण्टीजेन्स ऐसे रासायनिक पदार्थ है जो प्रतिरक्षी तन्त्र अर्थात् एण्टीबॉडीज को उत्तेजित करते हैं। ये अमीनो अम्लों या कार्बोहाइड्रेट्स से मिलकर बने होते हैं तथा इनमें एक या अधिक ऐण्टोजेनिक डिटरमिनेट क्षेत्र होता है। ऐण्टीबॉडी दो या चार पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं से मिलकर बनी होती है और प्रायः प्रोटीन ही होती है। ये प्रायः ऐण्टीजेन्स या अन्य पदार्थों की उत्तेजना के बाद ही बनती है।
प्रश्न 2. कुछ सामान्य वाइरस उत्पादित रोगों को नामांकित कीजिये।
उत्तर- वाइरस द्वारा उत्पन्न होने वाले रोग-चेचक (small pox). हरपीज (herpes), आर्थराइटिस (arthritis), डी०एन०ए० वाइरस (DNA virus) द्वारा तथा पोलियो (polio), डेंग्यू ज्वर (dangue fever), कर्णफेर (mumps), खसरा (measles), रेबीज (rabies) आदि आर०एन०ए० वाइरस (RNA virus) द्वारा उत्पन्न होते हैं।
प्रश्न 3. टिटेनस किस प्रकार शरीर में प्रवेश करता है?
उत्तर- टिटैनस एक अत्यधिक भयंकर एवं घातक रोग है जिसमें अधिकांश व्यक्तियों की मृत्यु हो जाती है। यह रोग एक विशेष प्रकार के जीवाणु क्लॉस्ट्रीडियम टिटैनी (Clostridium tetani) के शरीर में प्रवेश करने से होता है। टिटैनस रोगाणु मुख्य रूप से घोड़े की लीद, गोबर तथा खाद में पाये जाते हैं। जब कभी कहाँ चोट लग जाये या कट जाये तो उस स्थान से टिटेनस के रोगाणु रुधिर में प्रवेश कर जाते हैं।
प्रश्न 4. एड्स रोग के रोगजनक की खोज के बारे मे बताए।
उत्तर: एच०आई०वी०(HIV = Human Immunodeficiency Virus):
सन् 1981 में अमेरिका में एक सर्वे किया गया जिससे ज्ञात हुआ कि वहाँ रहने वाले कुछ समलैंगिक युवकों में, जिन्हें मादक पदार्थ लेने की आदत थी, त्वक कैन्सर तथा न्यूमोनिया) जैसे घातक रोग होने लगे। इन युवकों में इन रोगों के प्रति प्रतिरक्षण क्षमता भी बहुत कम हो चुकी थी। सन् 1984 में रॉबर्ट गैलो ने बताया कि यह रोग एक अज्ञात रीट्रोवाइरस श्रेणी के वाइरस के संक्रमण से होता है। सन् 1986 में वाइरस नामकरण को अन्तर्राष्ट्रीय समिति (International Community on Virus Nomenclature = ICVN) ने इस वाइरस को मानव प्रतिरक्षा अपूर्णता वाइरस (Human Immunodeficiency Virus = HIV) नाम दिया।
प्रश्न 5. मानव रोगों के प्रकार बताए।
उत्तर: मनुष्य में उत्पन्न होने वाले रोगों को दो श्रेणियां निम्नलिखित है
1. आनुवंशिक या जन्मजात रोग - मनुष्य में ये रोग जोन्स या गुणसूत्रों में गड़बड़ी के कारण हो जाते है और पीढ़ी-दर-पीढ़ी स्थानान्तरित होते रहते हैं। हीमोफीलिया, रतौंधी, रंजकहीनता, ऐल्केप्टोनूरिया, सिकिलसेल ऐनीमिया, डाइबिटीज आदि ऐसे ही आनुवंशिक या जन्मजात रोगों के उदाहरण है।
2. उपार्जित रोग —ये रोग मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं—
(i) संक्रामक रोग – ये रोगाणुओं के संक्रमण से उत्पन्न होने वाले रोग हैं, जो एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य में फैल सकते हैं। क्षय (टी० बी०), फ्लू (इन्फ्लुएन्जा), नजला, जुकाम, मलेरिया, चेचक, प्लेग, खसरा, डिफ्थीरिया, उपदेश, सुजाक, एड्स, आदि संक्रामक रोगों के उदाहरण है।
(ii) असंक्क्रामक रोग —ये ऐसे रोग होते हैं जिनका संक्रमण एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं होता है। क्वाशरकोर, मेरेस्मस, रिकेट्स, ऐनीमिया (रक्ताल्पता), एलर्जी, आन्त्र ज्वर, हृदय रोग, कैन्सर, रतौंधी, बेरी-बेरी, मधुमेह, गठिया रोग, वर्णान्यता आदि असंक्रामक रोगों के उदाहरण है।
प्रश्न 6. संक्रामक रोगों से बचाव के उपाय बताए।
उत्तर: संक्रामक रोगों से बचाव के उपाय: संक्रामक रोग किसी न किसी माध्यम से शरीर के अन्दर प्रवेश करते हैं; अतः इनको रोकने के लिए अग्रलिखित उपाय हैं-
(i) रोग के वाहक (साधन) को नष्ट करना होगा अथवा उसका शुद्धिकरण या निःसंक्रमण आवश्यक है।
(ii) रोगाणु नष्ट करने के लिए कोई प्रभावी औषधि का उपयोग करना आवश्यक है। (iii) रोगाणु द्वारा शरीर में वृद्धि के प्रति शरीर को प्रतिरोधित करना चाहिये। इसके लिए संक्रामक रोगों के टीके आदि लगाने की व्यवस्था होनी चाहिये। संक्रामक रोग तेजी से फैल सकते हैं और महामारी का रूप धारण कर लेते हैं। अत: इस प्रकार के रोग कहीं पर किसी भी व्यक्ति में हो उसकी तुरन्त और विस्तृत सूचना आवश्यक है, ताकि उसको फैलने से रोकने के अधिकाधिक उपाय किये जा सके।
प्रश्न 7. निमोनिया रोग का संक्षिप्त मे वर्णन करे।
उत्तर: कई प्रकार के जीवाणु निमोनिया उत्पन्न करते हैं। प्रमुख है—–डिप्लोकोकस निमोनी (Diplococcus pneumoniae), स्ट्रेप्टोकॉक्स निमोनी (Streptococcus pneumoniae), हीमोफिलस इन्फ्ल्यूऐन्जी (Haemophilus influenzae)। इस रोग में फेफड़ों में वायु कोष्ठ संक्रिमत होते हैं तथा संक्रमण के चलते इनमें अत्यधिक मात्रा में श्लेष्म भर जाता है, सांस लेने में कठिनाई होती है। कभी-कभी यह स्थिति अत्यन्त भयानक स्वरूप प्राप्त कर लेती है, ज्वर, ठिठुरन, खांसी, भयंकर सिरदर्द, अत्यधिक थकान अधिक गम्भीर स्थिति में होठ, नाखून आदि नीले पड़ना आदि लक्षण देखे जा सकते हैं। नशीले पदार्थ सेवन करने वालों को यह रोग आसानी से हो जाता है। संक्रमण प्रमुखतः रोगी द्वारा सांस, छींक आदि में छोड़े गये बिन्दुकों से, रोगी के बर्तनों इत्यादि को इस्तेमाल करने से होता है।
प्रश्न 8. इंफ्लुएंजा रोग के लक्षण लिखे।
उत्तर: इन्फ्लूएन्जा: संक्षेप में से फ्लू (flue) कहते हैं। यह वायु के माध्यम से बहुत तेजी से फैलने वाला विषाणु जनित रोग हैं। इस रोग के विषाणु नाक की झिल्ली तथा श्वासनली को प्रभावित करते हैं। फ्लू के विषाणु स्वस्थ मनुष्य के शरीर में रोगों के खाँसने, छींकने, हँसने तथा जोर से बोलने पर वायु के माध्यम से तथा रोगी के रुमाल व तीलिया आदि का प्रयोग करने से पहुँच जाते हैं। रोग के लक्षण-रोग के प्रारम्भ में छींक, जुकाम, सिर दर्द, नेत्रों में पीड़ा के साथ नाक बन्द हो जाती है और साँस लेने में भारी कठिनाई होती है। धीरे-धीरे शरीर के अन्य भागों में पीड़ा होने लगती हैं। नेत्रों व नाक से पानी बहने लगता है। शरीर बेचैन और कमजोर हो जाता है। बाद में ज्वर भी आ जाता है जो 3-4 दिन में उतर जाता है। कभी-कभी खाँसी बाद में निमोनिया तथा ब्रॉन्काइटिस में भी बदल जाती है।
प्रश्न 9. प्लसमोदिउम के जीवन चक्र व संक्रमण को संक्षिप्त मे बताए।
उत्तर: प्लाज्मोडियम का जीवन चक्र : मलेरिया परजीवी अर्थात् प्लाज्मोडियम वाइवैक्स का जीवन चक्र दो पोषदों में पूर्ण होने के कारण द्विपोषदीय कहलाता है। मनुष्य प्लाज्मोडियम का प्राथमिक अथवा मुख्य पोषद है जबकि मादा ऐनोफेलीज मच्छर इसका द्वितीय पोषद्र) है। इसका अलैंगिक जनन अर्थात् शाइजोगॉनी मनुष्य में तथा लैंगिक जन व बीजाणुजन मादा ऐनोफेलोज में पूर्ण होता है।
संक्रमण -म मादा ऐनोफेलीज अपने भेदक एवं चूषक मुखीय उपांगों द्वारा मनुष्य का रुधिर चूसती है। इससे पूर्व वह रुधिर में थोड़ा-सा लार मिलाती है। इसकी लार के साथ हजारों अतिसूक्ष्म स्पोरोज्वॉएट्स मनुष्य के रुधिर में प्रवेश कर जाते हैं। स्पोरोज्वॉएट (sporozoite) लगभग 60-15 लम्बा हँसियाकार तथा एककेन्द्रकीक होता है। इसके चारों ओर एक कड़ा एवं लचीला पेलिकल होता है।
प्रश्न 10. सहज प्रतिरक्षा के घटक कौन कौन से है?
उत्तर: सहज या अविशिष्ट प्रतिरक्षा तथा उसके घटक:
किसी संक्रमण या आक्रमण से बचाने के लिए हमारे शरीर में कई रक्षा प्रणालियाँ होती है जिनमें से अविशिष्ट प्रतिरक्षा प्रणाली भी एक है। इसके अन्तर्गत दो प्रकार के प्रतिरक्षा तन्त्र आते हैं-बाह्य मार्ग रोधन तथा अन्तः मार्ग रोधन। बाह्य मार्ग अवरोधन का कार्य हमारी त्वचा तथा श्लेष्मिक कलायें करती है। भीतरी प्रतिरक्षी घटकों में
(1) प्राकृतिक विनाशी कोशिकाये
(2) प्रतिरोगाणु पदार्
(3) भक्षी कोशिकायें
(4) प्रदाह
(5) ज्वर (fever) आदि आते हैं।
प्रश्न 11. इंटेरफेरॉनस क्या होते है परिभासित करे।
उत्तर: इण्टरफेरोन्नर: कशेरुकी जन्तुओं में वाइरस से संक्रमित कोशिकाओं द्वारा सटवृत एक गलीकोप्रोटीन पदार्थ है जो इन कोशिकाओं को वायरस से संक्रमण के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करते हैं। इण्टरफेरोन के उपयोग काइरस संक्रमण के लिए रोग निवारक तथा निरोधक औषधियों के रूप में किया जाता है। आइसक्स तथा लिण्डनमैन ने सन् 1957 में इस प्रकार की प्रोटीन का पता लगाया और चूंकि इसने अन्तःकोशिकीय विषाणुओं के गुणन को रोका इसलिए इसको इण्टरफेरोन कहा गया। ऐसा समझा जाता है कि इण्टरफेरोन्स विषाणु केन्द्रकीय अम्ल संश्लेषक तन्त्र को बाधित करता है, किन्तु यह किसी प्रकार भी कोशिका के उपापचय में कोई विघ्न नहीं डालता है। यह भी निश्चित हो चुका है कि इण्टाफेरोन्स कोशिका के बाहर उपस्थित विरिऑन्स आदि को किसी प्रकार भी प्रभावित नहीं करते हैं, न ही संक्रमण रोकने में किसी प्रकार सक्षम हैं। ये कोशिका के अन्दर ही क्रिया करते हैं अर्थात् केवल अन्तः कोशिकीय क्रियायें ही करते हैं।
प्रश्न 12. b lymphocyte के बारे म बताए।
उत्तर: बी - लिम्फोसाइट्स: बी-लिम्फोसाइट्स को बी-कोशिकायें भी कहते हैं। यह पक्षियों (चूजों) के निचले जठरान्त क्षेत्र में स्थित एक ग्रन्थि फैब्रिसी प्रपुटी में विकसित होती है। B-cells की सतहों पर कुछ रासायनिक पदार्थ उपस्थित होते है, जिनकी सहायता से इनमें एवं T-cells में अन्तर किया जा सकता है। इन लसीकाणुओं की जीवन अवधि 5-7 दिन होती है, जबकि T-cells कई माह अथवा वर्षों तक जीवित रह सकती है। परिसंचारी लसीकाणुओं में लगभग 65-80% T-cells तथा शेष में अधिकतर B-cells तथा कुछ प्रतिशत में दोनों ही प्रकार की अपरिपक्व कोशिकायें होती है। B-cells तरल प्रकृति की प्रतिरक्षा अनुक्रिया करती हैं। B-कोशिकाओं के पृष्ठीय घटकों का उत्पादन जीन्स के नियन्त्रण में रहता है, जिन्हें प्रतिरक्षित अनुक्रिया जीन्स कहते हैं। मनुष्यों में प्रतिरक्षित अनुक्रिया जीन्स विभिन्न गुणसूत्रों पर स्थित होते हैं।
प्रश्न 13. एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटेलिस क्या होता है?
उत्तर: नवजात शिशुओं में Rh फैक्टर के प्रति प्रतिरक्षी (एण्टीबॉडी) उत्पादन के कारण होने वाला यह व्यतिक्रम Rh पुरुष व Rh स्त्री से उनकी सन्तान Rh" होने पर होता है। प्रसव के समय जब माता एवं शिशु का रुधिर मिलता है तो माँ के रुधिर में Rh factor प्रति प्रतिरक्षी बनने लगते हैं इससे इस (प्रथम) शिशु को तो प्रायः कोई हानि नहीं होती किन्तु दूसरा शिशु भी Rh हुआ तो माता के रुधिर में उपस्थित प्रतिरक्षी शिशु की लाल रुधिर कणिकाओं (RBCs) को नष्ट करने लगते. और गम्भीर हीमोलिटिक रक्ताल्पता से शिशु की मृत्यु हो सकती है।
प्रश्न 14. SCID को परिभाषित करे।
उत्तर: उग्रसंयुक्त प्रतिरक्षा न्यूनता: यह जन्मजात अपसामान्यता है जिसमें बाल्यावस्था में ही T एवं B लिम्फोसाइट्स नहीं होते हैं। अतः ऐसे शिशुओं में कोई भ संक्रमण आसानी से हो जाता है तथा यह अति भयानक स्वरूप धारण कर सकता है। T-लिम्फोसाइट्स के अभाद में इसे डाइ-ज्योर्ज सिण्ड्रोम एवं B लिम्फोसाइट्स के अभाव में एगमैग्लूलीनीमिया रोग कहते हैं।
प्रश्न 15. एड्स पर नियन्त्रण के उपाय बताए।
उत्तर: 1. एदस पर नियंत्रण के लिए अभी तक कोई टीका (vaccine) आदि नहीं बनायी जा सकी है।
2. किसी अनजाने व्यक्ति के साथ यौन सम्बन्ध स्थापित नहीं करना चाहिए तथापि सम्भोग के समय कण्डोम का प्रयोग किया जाना चाहिए।
3. एक बार उपयोगित इन्जेक्शन की सुई का प्रयोग दुबारा नहीं किया जाना चाहिए।
4. एड्स संक्रमित व्यक्ति द्वारा किसी भी तरह से रुधिर दान नहीं करना चाहिए।
5. रुधिर आधान से पूर्व रुधिर का HIV मुक्त होना आवश्यक है अर्थात् इसकी पूर्ण जाँच अनिवार्य होनी चाहिए।
6. एड्स पीड़ित स्त्री को माँ नहीं बनने देना चाहिए।
प्रश्न 16. सक्रिय प्रतिरक्षा को परिभाषित कीजिए।
उत्तर: चेष्टया सक्रिय प्रतिरक्षा : शरीर की अपनी प्रतिरक्षा सक्रिय होती है क्योंकि इनके लिए उपयुक्त एण्टीबॉडीज का संश्लेषण स्वयं शरीर में हो होता है। यह स्थायी प्रतिरक्षा रोगग्रस्त हो जाने पर एवं इसके ठीक हो जाने के बाद विकसित होती है। यह प्रतिरक्षा जन्मजात होती है। सूक्ष्मजीवों के तनुं विलयन या मृत सूक्ष्मजीवी या रोग उत्पन्न करने वाले उनके उपापचयी पदार्थों का इंजेक्शन देने से भी सक्रिय प्रतिरक्षा विकसित की जाती है। इन्हें शॉट (shot) कहते हैं जो हैजा, खसरा, डिफ्थीरिया, रेबीज, टाइफॉइड, कुफर खाँसी आदि रोगों से प्रतिरक्षा के लिए दिये जाते है।
प्रश्न 17. अक्रिय व सक्रिय प्रतिरखशा मेअंतर स्पष्ट करे।
उत्तर:
सक्रिय प्रतिरक्षा | निष्क्रिय प्रतिरक्षा | |
1. 2. 3. 4. 5. | जिस मनुष्य के शरीर में सक्रिय प्रतिरोध क्षमता उत्पन्न करनी होती है, उसी के शरीर में प्रतिजन प्रविष्ट कराये जाते हैं। प्रतिजन के उद्दीपन से कुछ समय के बाद उस मनुष्य के शरीर में प्रतिरक्षी उत्पन्न हो जाते हैं। प्रतिरक्षियों के बनने से उस मनुष्य के शरीर में प्रतिरोध क्षमता या असंक्राम्यता उत्पन्न हो जाती है। इस प्रतिरोध क्षमता के उत्पन्न होने में समय लगता है। यह प्रतिरोध क्षमता अधिक समय तक स्थित रहती है। | जिस मनुष्य के शरीर में प्रतिरोध क्षमता उत्पन्न करनी न होती है, उसके शरीर में नहीं अपितु किसी दूसरे प्राणी के शरीर में प्रतिजन प्रविष्ट कराये जाते हैं। जिस. प्राणी के शरीर में प्रतिजन प्रविष्ट कराये जाते हैं। उसके शरीर में कुछ समय के बाद प्रतिरक्षी उत्पन्न हो जाते हैं। प्राणी का प्रतिरक्षीयुक्त सीरम मनुष्य के शरीर में प्रविष्ट करा देने से उसको प्रतिरोध क्षमता या असंक्राम्यता प्राप्त हो जाती है। इस प्रकार की प्रतिरोध क्षमता मनुष्य को सीरम का इन्जेक्शन देते ही प्राप्त हो जाती है। यह प्रतिरोध क्षमता शरीर में शीघ्र ही समाप्त हो जाती है। |
प्रश्न 18. सक्रिय प्रतिरोध क्षमता के स्त्रोत बताए।
उत्तर: प्रतिरोध क्षमता का स्रोत : इस प्रकार की प्रतिरोध क्षमता शुद्ध एवं मूल प्रतिजनों के शरीर में प्रविष्ट कराने के उपरान्त उत्पन्न होती है। प्रतिजन वैक्सीन (टीका) अथवा मृतक या जीवित पूर्ण रूप से क्रियाशील जीवाणु/विषाणु होते हैं।
प्रकृतिक: यह प्रतिरोध क्षमता जीवित एवं पूर्ण रूप से क्रियाशील सूक्ष्मजीव के द्वारा निर्मित होती है, जो प्राकृतिक रूप से रोग उत्पन्न करने की क्षमता रखते हैं।
कृत्रिम : यह प्रतिरोध क्षमता जीवित मृतक या क्षीण क्रिया वाले सूक्ष्मजीवों के कृत्रिम रूप से प्राणियों के शरीर में प्रविष्ट कराने के उपरान्त उत्पन्न होती है।
प्रश्न 19. केन्सर रोग पर टिप्पणी कीजिए।
उत्तर: कैन्सर :
रोग तथा रोग का कारण- इस रोग में कोशिका विभाजन अनियन्त्रित, अनियमित तथा तीव्र गति से होता है। ये कोशिकायें क्रियाकारी भी नहीं होती अर्थात् इनका पूर्ण रूप से विभेदीकरण भी नहीं होने पाता है। ये कोशिकायें अन्य कोशिकाओं को पोषक पदार्थों को ग्रहण नहीं करने देतों जिससे उनकी मृत्यु होने लगती है। इस प्रकार के तीव्र कोशिका विभाजन से उस स्थान विशेष पर गाँठ या अर्बुद बन सकती है।
शरीर में कोशिका वृद्धि और विभेदन अत्यन्त नियमित एवं नियन्त्रित क्रिया विधि के द्वारा होती है। प्रसामान्य कोशिकाओं में यह गुण जिसे संस्पर्श संदमन कहते है, दूसरी कोशिकाओं को अनियन्त्रित वृद्धि को संदमित करता है। कैन्सर कोशिकाओं में इस प्रकार का संदमन समाप्त हो जाता है। कैन्सर का कारण कोशिकाओं में उपस्थित ऑन्कोजीन्स का सक्रिय होना माना जाता है। यद्यपि ऑन्कोजीन्स सभी कोशिकाओं में होती हैं, किन्तु सामान्यतः ये निष्क्रिय होती है। किसी विशेष कारण से ये सक्रिय हो सकती है।
प्रश्न 20. मादक द्रव्यों का शरीर पर दुष्प्रभाव बताए।
उत्तर: सभी मादक पदार्थ मनुष्य के लिए अत्यन्त हानिकारक होते हैं क्योंकि मनुष्य धीरे-धीरे इनका आदी हो जाता है और बाद में इच्छा होने पर भी सरलतापूर्वक इन्हें नहीं छोड़ पाता। प्रत्येक मादक पदार्थ मनुष्य के मस्तिष्क एवं स्नायविक संस्थान पर सीधा प्रभाव डालता है; अतः इसके प्रयोग से उसकी कार्यक्षमताओं में गिरावट आने लगती है और शनैः शनैः उसका शरीर जर्जर होता चला जाता है। वह समय से पहले ही स्वास्थ्य गंवा बैठता है और कम आयु में वृद्ध प्रतीत होने लगता है। ऊपर से दिखायी देने वाली फुर्ती व उत्तेजना अन्दर ही अन्दर शरीर को कमजोर मे व खोखला बनाती रहती है। फिर तो व्यक्ति भोजन की अपेक्षा मादक पदार्थों को अधिक महत्त्व देने लगता है। इससे उसका स्वास्थ्य तो नष्ट होता ही है उसके धन की भी हानि होती है तथा नैतिक पतन होने लगता है, वह बिल्कुल विवेकशून्य हो जाता है। विभिन्न मादक पदार्थ स्वास्थ्य पर विभिन्न प्रकार से बुरा प्रभाव डालते हैं। कई बार तो यकृत (liver), गुर्दे (kidneys) आदि शरीर के विशिष्ट शोधक अग ही विकृत व रोगों हो जाते है। अधिकतर लोगो में इनके रोगों का स्वरूप लाइलाज होता है।
प्रश्न 21. मादक पदार्थ अफीम का शरीर पर प्रभाव बताए।
उत्तर: अफीम का प्रभाव — अफीम पॉपी या पोस्त नामक पौधे के फल (सम्पुट से निकले रबर क्षीर, सफेद दूध जैसे पदार्थ से बनाये जाने वाला मादक पदार्थ है। इसके सेवन से शरीर पर प्रत्यक्ष रूप से अत्यधिक दुष्प्रभाव पड़ता है अतः इसका प्रयोग गैरकानूनी माना शरीर पर इसके दुष्प्रभाव निम्नलिखित है-
(i) व्यक्ति आलसी हो जाता है और उसे हर समय नींद आती रहती है।
(ii) व्यक्ति की आँखों की चमक कम हो जाती है और अपने शरीर से उसका नियन्त्रण पूरी तरह समाप्त हो जाता है।
(iii) व्यक्ति की शारीरिक और मानसिक शक्तियाँ नष्ट होने लगती है और आँखे कमजोर हो जाती है।
प्रश्न 22. मनुष्य में मलेरियल आक्रमण होने के दौरान कंपकपी का कारण बताइए। दुर्दम मलेरिया के रोगकारक का नाम बतड़ाए।
उत्तर- मलेरिया परजीवी के मनुष्य में संक्रमण होने पर प्लाज्मोडियम के ट्रोफोज्याएट यकृत कोशिकाओं में गोन करके असंख्य मीरोज्वाएट का निर्माण करते हैं। ये मौरोज्याएट असंख्य लाल रुधिर कणिकाओं का विनाश करते हैं तथा एक पदार्थ हीमोज्वाइन उत्पन्न होता है। इसकी उत्पत्ति एवं RBC के विनाश के कारण मनुष्य को कंपकपी उठती है। दुर्दम मलेरिया प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम द्वारा होता है।
प्रश्न 23. सिफ़लिस रोग पर टिप्पणी दे
उत्तर: आतशक या उपदंश (syphilis): ट्रेपोनीमा पैलीडम नामक जीवाणुओं द्वारा होने वाला रोग है। इस रोग में जनन तन्त्र के विभिन्न भागों में घाव हो जाते है जो ठीक नहीं होते हैं। शरीर के अन्य भागों में रोग के विभिन्न प्रभाव पड़ते हैं। उपचार के रूप में प्रतिजैविकों का प्रयोग कराया जाता है।
रोग से बचाव के लिए:
(1) संक्रमित व्यक्ति के साथ यौन सम्पर्क नहीं करना चाहिए। साथ ही सामान्यतः भी यौन सम्पर्क में निरोध (कण्डोम) का प्रयोग किया जाना चाहिए।
(i) दूषित इन्जेक्शन की सुई का प्रयोग नहीं करना चाहिए।
(iii) संक्रमित व्यक्ति का रुधिर किसी अन्य व्यक्ति को नहीं चढ़ाना चाहिए।
प्रश्न 24. अर्जित प्रतिरक्षा किस प्रकार से प्राप्त की जाती है?
उत्तर: असंक्राम्यता प्राप्त करना: इन्जेक्शन लगाकर अथवा अन्य किसी विधि से रोगाणुओं द्वारा उत्पन्न पदार्थ अथवा रोगाणुओं को ही स्वस्थ शरीर में प्रविष्ट करा दिया जाता है। इससे शरीर में स्वतः ही ये प्रतिरक्षी पदार्थ उत्पन्न हो जाते हैं जिनसे उन विशेष रोगों को रोका जा सकता है। बी०सी०जी०, डी०पी०टी०, चेचक आदि के टीके द्वारा असंक्राम्यता शिशु अवस्था में हो अर्जित की जाती है। इसी प्रकार पोलियो की दवा पिलाकर असंक्राम्यता अर्जित की जाती है।
प्रश्न 25. मलेरिया से बचने के उपाय बताए।
उत्तर: उपचार - रोगी को पूर्ण विश्राम देना चाहिए। कुनैन ही इस रोग की एकमात्र औषधि समझी जाती है, जो लगभग सभी दवाओं में किसी न किसी रूप में होती है। कुछ चिकित्सक इंजेक्शन लगाकर भी इसका सफल इलाज करते हैं।
बचने के उपाय- 1. इस रोग में रोगी को कुनैन, कैमोकुइन या पैल्युद्दिन आदि औषधियों को खिलाना चाहिए। ये सब मलेरिया नाशक दवायें है। 2. मच्छरों का नाश करना आवश्यक है। अतः गन्दे नालों, कूड़ेदानों तथा गड्ढों में (जहाँ मच्छर अण्डे देते हैं) मिट्टी का तेल छिड़क देना चाहिए जिससे मच्छर अथवा उनके अण्डे वहीं नष्ट हो जाये तथा घरों में या अन्य स्थानों में भी जहाँ मच्छरों के निवास का सन्देह हो, डी० डी० टी० या अन्य दवाओं को छिड़ककर मच्छरों का नाश करना चाहिए।
हिंदी के सभी अध्याय के महत्वपूर्ण प्रशन उत्तर के लिए अभी Download करें Vidyakul App - Free Download Click Here